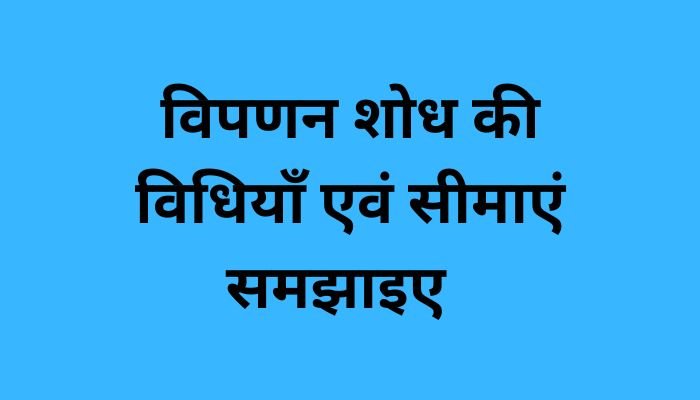
विपणन शोध की विशिष्ट तकनीकें तथा विधियाँ
विपणन शोध, विपणन समस्याओं के समाधान में उपयोगी सूचनाओं की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग की एक प्रक्रिया है। इन सूचनाओं को विभिन्न पद्धतियों एवं तकनीकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि विपणन समस्याओं का क्षेत्र अति व्यापक है। समस्याओं के समाधान हेतु समय-समय पर नयी-नयी विधियाँ अपनाई जाती है, जो हैं
(1) पैनल विधि-विपणन शोध में पैनल का अर्थ एक ही उत्तरदाता से दो या अधिक बार साक्षात्कार करके तथ्य संकलन करने से है। पैनल के दो प्रकार होते हैं-
(i) निरन्तर पैनल जिसमें सदस्य द्वारा निर्दिष्ट व्यवहार को नियमित सूचित किया जाता हैं।
(ii) अन्तराल पैनल में चयनित सदस्य शोधकर्त्ता कम्पनी को समय-समय पर सूचना है, देने हेतु सहमत हो जाते हैं। लेकिन ऐसी सूचना माँगे जाने पर ही दी जाती है।
विपणन शोध की इस तकनीक में उपभोक्ता पैनल का विशेष महत्त्व होता है, जिसमें साक्षात्कार के बिना जन सामान्य की राय मापी जाती है। सामान्यतः इस तकनीक में दैवनिदर्शन प्रणाली द्वारा शोध के क्षेत्र के अनुसार 500-5000 परिवारों की सूची बनायी जाती है। सूची के सदस्य नियमित रूप से खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दवाइयाँ आदि के क्रय विवरण भेजते रहते हैं। ऐसे विवरण से आयु, लिंग, आय आदि के आधार पर वर्गीकृत उपभोक्ताओं द्वारा क्रप की गयी ब्राण्ड का आकार तथा इकाइयों, क्रय मूल्य, क्रय का स्थान, समय और कारण आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है।
(2) उत्पाद परीक्षण-उत्पाद परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें निर्माता नये उत्पाद की ओर ग्राहक के दृष्टिकोण को पहले से ही निर्धारित करने का प्रयास करता है। विपणन शोध करने के लिए दो प्रकार के उत्पाद परीक्षण किये जाते हैं— (i) तकनीकी परीक्षण तो निरपेक्ष एवं सापेक्षिक रूप में किया जाता है, (ii) उपभोक्ता परीक्षण में उत्पाद का वास्तविक उपभोक्ता एक व्यक्ति होता है जो उपभोग के बाद उत्पाद निर्माता को उसके उत्पादन के संबंध में सही जानकारी देने की स्थिति में होता है क्योंकि उत्पाद का क्रेता एवं अन्तिम उपभोक्ता वही है। उपभोक्ता परीक्षण में इन चार कदमों का उपयोग किया जाता है–
(i) उत्पाद के विचार का परीक्षण किया जाता है। जिस उत्पाद पर विचार किया जाने वाला है, उसके संबंध में कुछ पूर्व सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है।
(ii) जब कुछ चुने हुए ग्राहकों को उत्पाद प्रयोगात्मक परीक्षक कार्य सौंप दिया जाता है तो वे प्रयोगशाला जैसी दशाओं में उसका परीक्षण करते हैं।
(iii) पूर्व परीक्षण के पश्चात् प्रारम्भिक बाजार परीक्षण किया जाता है, जिससे बाजार की स्थिति की जानकारी हो जाती है।
(iv) अंत में, उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करने के पश्चात् कुछ समय तक विश्राम दिया जाता है और यह जानकारी की जाती है कि ग्राहकों के द्वारा इसे कहाँ तक स्वीकार किया गया है।
(3) ब्राण्ड बेरोमीटर – प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अपने उत्पादों को एक पहचान चिह्न प्रदान करती है ताकि उन्हें तुरन्त एवं सरलता से पहचाना जाना जा सके और दूसरे उत्पादकों के उत्पाद से पृथक् और श्रेष्ठ बतलाया जा सके। ब्राण्ड के चार प्रकार होते हैं— (i) व्यक्तिगत ब्राण्ड, (ii) समूहगत ब्राण्ड, (iii) पारिवारिक ब्राण्ड, (iv) बहु-ब्राण्ड।
जहाँ तक ब्राण्ड अवधारणाओं का प्रश्न है, अधिकांशतः धारणाएँ ब्राण्ड के साथ वास्तविक अनुभव से उसके विषय में इधर-उधर से सुनकर उसका निर्माण करने वाली कम्पनी को प्रतिष्ठा से, पैकिंग, विज्ञापन से प्रस्तुतीकरण के आकार, अन्तर्वस्तु और विशिष्ट माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
परीक्षण बाजार में ब्राण्ड बेरोमीटर या स्वीकरण की माप में तीन चरण होते हैं— (i) ब्राण्ड मान्यता, (ii) ब्राण्ड प्राथमिकता, (iii) ब्राण्ड आग्रह। इस प्रकार ब्राण्ड बैरोमीटर से उपभोक्ता प्राथमिकताओं, बाजार भाग विश्लेषण, कुल उपभोक्ता विक्रय, विपणन व्यूह रचना आदि का निर्धारण किया जा सकता है।
(4) फुटकर दुकानों की सामग्री सूची का अंकेक्षण— विपणन शोध की इस तकनीक का विचारों से न होकर, तच्चों से अधिक संबंध होता है। इसमें विभिन्न स्तरों पर नियमित अवधि से माल या सामग्री सूची तैयार की जाती है जिसके आधार पर उत्पाद की वास्तविक क्रय स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है।
जब शोधकर्त्ता को यह ज्ञात करना है कि व्यक्ति कुछ निश्चित वस्तुएँ ही क्यों खरीदते हैं तो यहाँ साक्षात्कार की अपेक्षा तथ्यात्मक सर्वेक्षण द्वारा उत्पादन की विभिन्न विशेषताओं के संबंध में विचार-विमर्श द्वारा महत्त्वपूर्ण तथ्यों को ज्ञात किया जाता है। ऐसा फुटकर स्तर पर सामग्री सूची के अंकेक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।
इस प्रकार के अंकेक्षण में निश्चित समयान्तर से विभिन्न स्टोर्स से ये सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं, जैसे—उपभोक्ताओं को विक्रय, फुटकर स्टोर्स द्वारा क्रय, प्रतिपूर्ति आपूर्ति, सभी वस्तुओं का वितरण, आउट ऑफ स्टॉक, विशेष फैक्ट्री मूल्य, वितरक का समर्थन आदि।
फुटकर स्टोर्स से सामग्री सूची के अंकेक्षण में ये बातें ज्ञात की जा सकती हैं-
(i) सामग्री सूची एवं विक्रय भाग के मध्य संबंध।
(ii) माल के लिए विभिन्न मूल्यों को वसूल करते हुए स्टोर में माल की गतिशीलता की तुलना।
(iii) किन उत्पादों का विक्रय, स्टोर में अधिक है ?
(iv) स्टॉक स्थिति, सैल्फ स्थिति एवं शैल्फ फैसिंग का विक्रय पर प्रभाव। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विपणन शोध की इस तकनीक के द्वारा प्राप्त सूचनाएँ या तथ्य काफी सीमा तक सही होते हैं।
(5) प्रयोगशाला दुकान— विपणन शोध की यह नवीनतम तकनीक है। इसके अन्तर्गत वास्तविक स्थिति में विपणन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम रूप से वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है और विपणन समस्या को उस कृत्रिम स्थिति में प्रयुक्त करके वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
ऐसी प्रयोगशाला दुकानों का प्रयोग पैकेज आकार के प्रति उपभोक्ताओं का दृष्टिकोण और मूल्य का कीमत के प्रति उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण को समझने हेतु किया जाता है।
विपणन शोध की इस तकनीक के बारे में विपणन प्रबंध विशेषज्ञ ने कहा कि “विपणन शोध में प्रयोगशाला दुकानों का प्रयोग नये उत्पाद के परीक्षण पैकेज, प्ररचना, विज्ञापन विषय और प्रतिलिपि के प्रारम्भिक परीक्षणों के साथ-साथ आधारभूत शोध अध्ययनों में भी प्रयोग किया जाता है।”
विपणन शोध की सीमाएँ (Limitations of Marketing Research)
विपणन शोध समस्याओं का समाधान नहीं करता है, बल्कि समस्याओं के समाधान में सुदृढ़ निर्णय लेने में सहायता करता है। इसलिए यह त्रुटि मुक्त नहीं है। अतः इसकी निम्नलिखित सीमाएँ बतलायी जा सकती हैं-
(1) समय की सीमा – विपणन शोध समय लेने वाली एक प्रक्रिया है किन्तु शोधकर्ता जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने का आग्रह करता है। परिणामतः पूरी सूचनाओं एवं तथ्यों के बिना ही शोध रिपोर्ट देने से निर्णय गलत होने की संभावना होती है।
(2) मानसिक भिन्नताएँ—प्रत्येक विपणनकर्त्ता की मानसिक भिन्नता होती है। कुछ पूर्वापेक्षित बातें ही शोध के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं।
(3) दक्षता की सीमा–यदि शोधकर्त्ता कुशल एवं निपुण है तो सही सूचनाएँ एकत्रित हो जाती हैं अन्यथा गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं।
(4) प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव-उत्पादक शोधकर्त्ताओं को एक लिपिक स्तर से ऊपर नहीं मानते हैं। इसलिए उनका पारिश्रमिक बहुत ही कम होता है जिससे वे अधिक आकर्षित नहीं होते हैं। इस प्रकार अप्रशिक्षित एवं अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा निकाले गये परिणाम भी विश्वसनीय एवं प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं।
(5) केवल एक मानसिक अध्ययन– विपणन शोध केवल एक मानसिक अध्ययन है। इससे परिवर्तन तो आते हैं किन्तु वह कई बार परिणाम व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं।
(6) धन की सीमितता- विपणन शोध में धन की कमी निर्धारित नमूने को छोटा कर देती है। परिणामस्वरूप कम उपभोक्ताओं से सम्पर्क किया जाता है, जो सत्यता के बारे में संदेह उत्पन्न करते हैं।
(7) पक्षपता की सीमा- यह पक्षपात से परे नहीं है। किसी वस्तु स्थिति या व्यक्ति के बारे में पहले से ही किसी प्रकार की धारणा उसके कार्य पर प्रभाव डालती है।
(8) आर्थिक लागत– विपणन शोध में उच्च प्रशिक्षित व्यक्ति एवं पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है इसलिए इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए संस्था को लागत के रूप में काफी राशि व्यय करनी पड़ती है।
