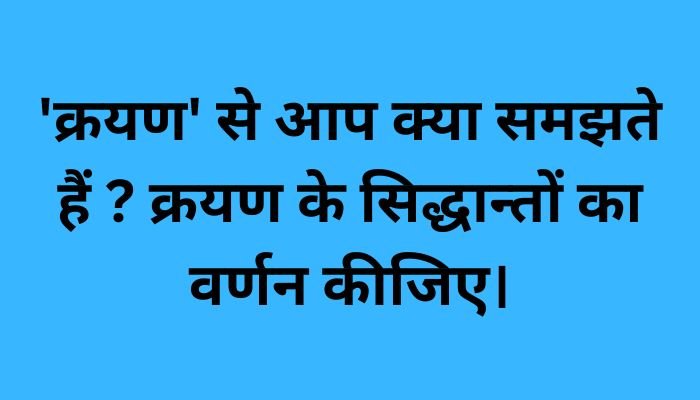
क्रयण का अर्थ
सामान्य शब्दों में, क्रय या खरीददारी से आशय निर्माण उपक्रमों में काम में आने वाली सामग्री की खरीद करने से है। संकुचित अर्थ में, क्रय का अभिप्राय किसी निश्चित मूल्य पर वांछित वस्तु को क्रय करना है। व्यापक एवं उचित अर्थ में सामग्री प्रबंध के दृष्टिकोण से क्रयण में उन सभी सम्बद्ध एवं पूरक क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है जो क्रय नियोजन, क्रय नीति के निर्माण, सामग्री पूर्ति स्रोतों की खोज, क्रय शर्तों आदि से संबंधित होती हैं।
(1) डॉक्टर वाल्टर्स के अनुसार, “क्रयण से आशय विपणन हेतु किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त सामग्रियों, मशीनों, उपकरणों एवं स्टोर्स की इच्छित किस्म के अनुरूप सही मात्रा में न्यूनतम कीमत पर क्रय द्वारा प्राप्ति से है।”
(2) वेस्टिंग, फाइन एण्ड जेन्ज के अनुसार, “क्रयण एक प्रबंधकीय क्रिया है ज केवल क्रय करने जैसे सरल कार्य तक ही सीमित नहीं है, वरन् समस्त सम्बद्ध एवं पूरक क्रियाओं को भी सम्मिलित करता है जो कि क्रय नियोजन एवं नीति कार्यों से संबंधित है।”
उपर्युक्त विवेचन से प्रकट है कि ‘क्रयण’ सामग्री प्रबंध का वह कार्य है जो आवश्यक कच्चे माल, मशीनों, यंत्रों, कल-पुर्जों, सुसज्जा व स्टोर्स सामग्री, अर्द्ध-निर्मित माल, अन्य आपूर्ति आदि को प्रमापित किस्म के अनुसार सही समय पर, सही मात्रा में, उचित स्त्रोत से प्राप्ति से संबंध रखता है।
बुनियादी रूप से क्रय दो प्रकार का होता है-
(1) पुनर्विक्रय हेतु क्रय एवं
(2) उपभोग अथवा रूपान्तरण हेतु क्रय
पुनर्विक्रय हेतु खरीद का कार्य सामान्यतः व्यापारियों और सटोरियों द्वारा किया जाता है। दूसरी ओर, उपभोग अथवा रूपान्तरण के लिए क्रय का कार्य औद्योगिक उपक्रमों, निर्माणी संस्थाओं, कारखानों आदि द्वारा किया जाता है। ऐसे औद्योगिक क्रेताओं को क्रय समस्याएँ भी भिन्न प्रकृति की होती हैं तथा उनकी खरीददारी विक्रय पूर्वानुमानों एवं उत्पादन अनुसूचियों पर आधारित होती है। अतः उनको उचित ‘क्रय नियेजन’ की आवश्यकता होती है। उनको वैज्ञानिक क्रय पर जोर देना होता है। अर्थात् औद्योगिक फर्मों को क्रय करते समय एक उत्पादक, वित्तीय प्रबंधक एवं विक्रय प्रबंधक की दृष्टि से भी विचार करना होता है। उन्हें दूरदर्शी एवं विवेकपूर्ण क्रय नियोजन के आधार पर खरीददारी करनी होती है।
क्रयण के सिद्धान्त (Principles of Purchasing)
क्रयण, नियोजन क्रय के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित होता है। नियोजन करने से पूर्व क्रय के प्रमुख सिद्धान्तों पर विचार कर लेना चाहिए। कुछ प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार है—
(1) सही किस्म का सिद्धान्त (Principle of Right Quality)— यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि अच्छे उत्पादों के निर्माण के लिए वांछित किस्म एवं गुणवत्ता वाली सामग्री को ही खरीदी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, क्रय की जाने वाली सामग्री उत्पादन लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। चूँकि निर्मित वस्तु की किस्म क्रय की गई सामग्री की किस्म पर निर्भर करती है, अत: सामग्री क्रय करते समय सामग्री के गुण-स्तर पर ध्यान देना आवश्यक है। सही किस्म के लिए सामग्री प्रबंधक को क्रय किये जाने वाले माल की किस्म के विनिर्देश (Specifications) पहले से निश्चित कर लेने चाहिए।
(2) सही मात्रा का सिद्धान्त (Principle of Right Quantity)—क्रय नियोजन का | एक मुख्य उद्देश्य कार्य के लिए सामग्री का निरन्तर प्रवाह बनाये रखना है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सामग्री को सही मात्रा में क्रय किया जाये। इसका अर्थ है कि सामग्री की मात्रा न बहुत अधिक क्रय की जानी चाहिए और न बहुत कम। अधिक मात्रा में सामग्री क्रय कर लेने पर पूँजी अनावश्यक रूप से अवरुद्ध हो जाती है और सामग्री की वहन लागतें (Carrying Costs) भी बढ़ जाती हैं। किन्तु कम मात्रा में सामग्री कय करने पर भी उत्पादन प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। अतः इन दोनों परिस्थितियों से बचने के लिए क्रय प्रबंधक को प्रत्येक सामग्री मद के लिए न्यूनतम एवं उच्चतम स्टॉक सीमा निश्चित कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मितव्ययी आदेश मात्रा (Economic Order Quantity) भी निश्चित कर ली जानी चाहिए।
( 3 ) सही समय का सिद्धान्त (Principle of Right time ) — क्रय नियोजन के समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी सामग्री मद को प्राप्त करने का सही समय वह बिन्दु है जब समाग्री का स्टॉक पूर्व निर्धारित न्यूनतम स्तर पर पहुँच जाये इस बिन्दु को छूते ही क्रय विभाग द्वारा सामग्री क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए ताकि कच्चे माल की जब भी जरूरत हो, वह उपलब्ध रहे। क्रय विभाग का कर्त्तव्य है कि ‘सुपुर्दगी की अनुसूची’ (Delivery Schedule) का ध्यान रखे। जब भी मूल्य में छूट का लाभ उठाने के लिए मौसमी क्रय का सहारा लिया जाता है, तब भी ‘सही समय’ का ध्यान रखा जाना चाहिए।
(4) सही स्त्रोत का सिद्धान्त (Principle of Rgiht Source)— क्रय नियोजन के समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि समाग्री का क्रय सही पूर्तिकर्त्ता से किया जाए जो अच्छी किस्म का माल नियत समय पर तथा उपयुक्त शर्तों पर प्रदान कर सके। क्रय के विभिन्न स्रोत होते हैं। किन्तु सही पूर्तिकर्त्ता का चयन उसकी पूर्ति शर्तों, साख, पूर्ति क्षमता, माल की गुणवत्ता, माल की नई किस्म तथा पिछले रिकार्ड आदि को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।
(5) सही स्थान का सिद्धान्त (Principle of Right Place)— क्रय नियोजन के समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि सामग्री की सुपुर्दगी सही स्थान पर ली जानी चाहिए ताकि सामग्री को परिवहन एवं हस्थन (Handling) लागतों में वृद्धि न हो। क्रय आदेश में सुपुर्दगी के स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। सामान्यतः माल की सुपुर्दगी का स्थान अपने कारखाने का गोदाम होना चाहिए। इसके लिए क्रय अनुबंध में ही इस शर्त का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।
(6) सही मूल्य का सिद्धान्त (principle of Right Price) क्रय नियोजन में सामग्री को उचित मूल्य पर क्रय किये जाने का ध्यान रखना चाहिए। उचित मूल्य का आशय सस्ते मूल्य से नहीं है। वास्तव में उचित मूल्य वह है जो क्रय की गई समाग्री की किस्म के अनुकूल हो। तथा क्रय की शर्तों, समय, प्रतियोगिता तथा बाजार दशाओं को देखते हुए उचित हो। क्रय क जाने वाली सामग्री का मूल्य प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद की कुल लागत को प्रभावित करता है। कच्चे माल का मूल्य अधिक होने पर वस्तु का उत्पादन भी अधिक होगा। अत: सामग्री का सही मूल्य | उसके लागत विश्लेषण के आधार पर ज्ञात किया जाना चाहिए।
