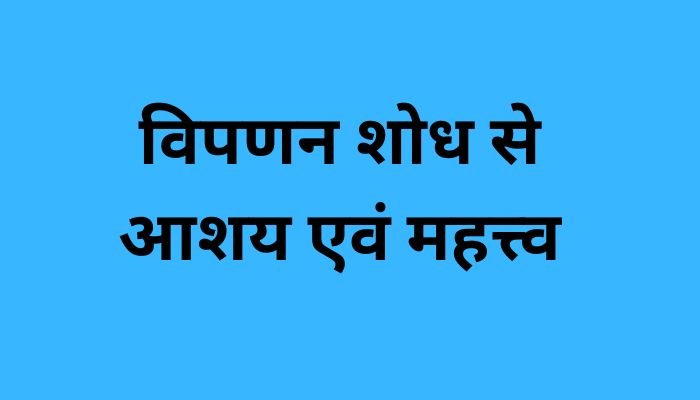
विपणन शोध का अर्थ एवं परिभाषाएँ
विपणन शोध अनुसंधान का अर्थ किसी भी समस्या का हल करने के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों का कठोरतापूर्वक पालन करने से है। अन्य शब्दों में, वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन में निर्णय और नियंत्रण संबंधी पद्धति में सुधार के लिए किया जाने वाला व्यवस्थित समस्या विश्लेषण मॉडल और तथ्य अन्वेषण को विपणन शोध कहते हैं।
विपणन शोध की निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ।
(1) रिचर्ड डी क्रिस्या के अनुसार, “विपणन क्षेत्र की कोई भी समस्या से संबंधित तथ्यों को किसी भी अध्ययन हेतु किये जाने वाले व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण एवं विस्तृत खोज ही विपणन शोध है।”
(2) लौरी एण्ड रॉबर्ट के शब्दों में, “विपणन समस्याओं के समाधान हेतु सूचनाओं की प्राप्ति के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयास विपणन अनुसंधान कहलाता है।”
(3) अमेरिकन मार्केटिंग ऐसोसियेशन के अनुसार, “विपणन शोध का आशय वस्तुओं एवं सेवाओं की विपणन संबंधित समस्याओं के बारे में आँकड़ों के व्यवस्थित संकलन, अभिलेखन, विश्लेषण एवं निर्वाचन से है।”
इस प्रकार विपणन शोध का आशय उन सभी सूचनाओं के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक एकत्रीकरण एवं विश्लेषण से है जिनके द्वारा वर्तमान एवं भावी विपणन समस्याओं का पता लगाया जा सके और समाधान हेतु सही निर्णय लेने में प्रबंधकों को सहायता मिल सके।
विपणन शोध का महत्त्व उपयोगिता (Importance of Marketing Research)
आधुनिक युग की प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति में व्यावसायिक संस्था का सुचारू संचालन हेतु वि विपणन प्रबंधक को काफी उपयोगिता है। इसके अभाव में ग्राहकों से संबंधित विभिन्न सूचनाएँ जैसे- ग्राहकों की इच्छा, बदलती हुई आवश्यकताओं, रुचियों एवं आदतों आदि की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसके अतिरिक्त विपणन शोध की उपयोगिता एवं महत्त्व को इन शीर्षकों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है-
(1) विक्रय पूर्वानुमान में सत्यता– उत्पादन के लिए कच्चा माल, श्रमिकों की मात्र, विपणन के लिए विक्रयकर्त्ताओं की संख्या, वित्त का प्रबंध आदि सभी बातें पूर्वानुमान पर आधारित होती हैं। यदि पूर्वानुमान गलत हो जाये तो संस्था को काफी हानि उठानी पड़ती है। अतः विपणन शोध, विक्रय पूर्वानुमान की सत्यता में वृद्धि कर संस्था के विभिन्न साधनों का अधिकतम संभव उपयोग करके लाभ में वृद्धि करता है।
(2) नये बाजारों की खोज- विपणन शोध से नये क्षेत्रों तथा ग्राहकों आदि का लगता है और नये-नये बाजारों की खोज संभव होती है। परिणामस्वरूप व्यावसायिक संस्था को नया कारोबार मिलता है और संस्था की उन्नति होती है।
(3) वस्तुओं के नये उपयोग— विपणन शोध की एक उपयोगिता यह भी है कि इससे यह पता चल जाता है कि क्या कम्पनी द्वारा उत्पादित वस्तु का उपयोग कम्पनी द्वारा सुझ गये कार्य के अतिरिक्त अन्य किन्हीं कार्यों में भी हो रहा है। फलस्वरूप उत्पादक/निर्माता को अपनी वस्तु के बारे में समझने का अवसर मिल जाता है और इसे एक नया क्षेत्र भी मिल जाता है।
(4) वस्तुओं में सुधार – विपणन शोध से ग्राहकों की रुचि तथा उनकी संतुष्टि का पता लग जाता है। यदि यह पता लगता है कि वस्तु के ग्राहक संतुष्ट नहीं हैं तो उसके कारणों/कमियों की जानकारी की जाती है और अपेक्षित सुधार का प्रयास किया जाता है।
(5) नियोजित उत्पादन-विपणन शोध का महत्त्व उत्पादन की दृष्टि से भी कम नहीं है क्योंकि-
(i) प्रतिस्पर्द्धा, उपभोक्ताओं की रुचि, उपभोक्ताओं की देय क्षमता और कुल माँग आदि का पता लगाया जाता है।
(ii) आकार, मूल्यों एवं गुणों में व्यापक परिवर्तन किये जा सकते हैं।
(iii) माँगों के अनुरूप कुल उत्पादन किया जा सकता है।
(iv) उपभोक्ताओं की रुचि एवं देय क्षमता के आधार पर उत्पदान किया जा सकता है।
(v) प्रशासनिक एवं उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है।
(6) वितरण व्यवस्था का मूल्यांकन— वितरण शोध करके वितरण व्यवस्था का यह पता लगाया जा सकता है कि वितरण व्यवस्था संतोषजनक है या नहीं। यदि वह संतोषजनक पता नहीं है तो उसमें आवश्यक सुधार किया जाता है। जिन स्थानों पर वस्तु की माँग है, वहाँ माँग के अनुरूप वितरण व्यवस्था भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जहाँ माँग अधिक है, वहाँ वितरण हेतु अतिरिक्त व्यवस्था की जा सकती है।
(7) विक्रय प्रबंध का मूल्यांकन एवं सुधार— विभिन्न क्षेत्रों के विक्रय प्रबंधक एवं विक्रयकर्त्ता की परस्पर तुलना की जाती है, जिससे कार्यकुशल एवं अकार्यकुशल विक्रेताओं तथा प्रबंधकों का पता चलता है। अकार्यकुशल प्रबंधकों तथा विक्रेताओं को प्रशिक्षण द्वारा सुधारा जाता है। इस प्रकार संस्था की कार्यकुशलता में सुधार होता है।
(8) ग्राहक से सम्पर्क स्थापित करने में सुविधा– वस्तुओं के ग्राहक दूर-दूर के क्षेत्रों में फैले होने के कारण इनकी आवश्यकता एवं इच्छाओं एवं उनकी उत्पाद के दृष्टिकोण का पता नहीं लग पाता है। ऐसी दशा में विपणनशोध द्वारा उत्पादक ग्राहकों से सम्पर्क करके उनकी अभिरुचियों का पता लगाते हैं और अनुकूल वस्तुओं का निर्माण कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
(9) माँग की प्रकृति की जानकारी- विपणन शोध से निर्माता को माँग की प्रकृति अर्थात् वह लोचदार है, कम लोचदार है, अधिक लोचदार है, अथवा लोचहीन है, का पता लग जाता है। इसके अतिरिक्त इससे यह भी पता लग जाता है कि माँग निरन्तर बनी रहने वाली या मौसमी। इस प्रकार विपणन शोध से दीर्घकालीन उत्पादन कार्यक्रम बनाने में मदद मिलती है।
(10) उपभोक्ताओं की दृष्टि से विपणन शोध उपभोक्ताओं की दृष्टि से भी काफी महत्त्व रखता है, क्योंकि—
(i) यह उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार उत्पादक को उत्पादन करने के लिए विवश करता है।
(ii) विभिन्न लागातों को घटाने में सहायक होता है जिससे वस्तुओं की कीमत कम की सकती है।
(iii) जनसाधारण को उन्नत वस्तुएँ उपभोग के लिए मिल जाती हैं, जबकि उपभोक्ता को प्रतियोगी मूल्य ही देने पड़ते हैं।
(iv) यह वस्तुओं में सुधार करने के लिए निर्माता को आवश्यक सलाह देता है।
(11) वितरण माध्यामों की कुशलता का मूल्यांकन- विपणन शोध से विक्रय मध्यस्थों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन हो जाता है और उसमें किसी भी प्रकार की कमी को दूर किया जा सकता है। परिणामतः कम्पनी की वितरण व्यवस्था संतोषजनक है या नहीं, का पता लग जाता है।
(12) राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग- विपणन शोध राष्ट्र के लिए भी उपयोगी है। इसमें राष्ट्रीय साधनों के सदुपयोग में सहायता मिलती है। व्यर्थ के व्ययों की बचत होती है। आधुनिकतम एवं नवीनतम वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है जो विदेशी व्यापार को बढ़ाने में सहायक होता है।
