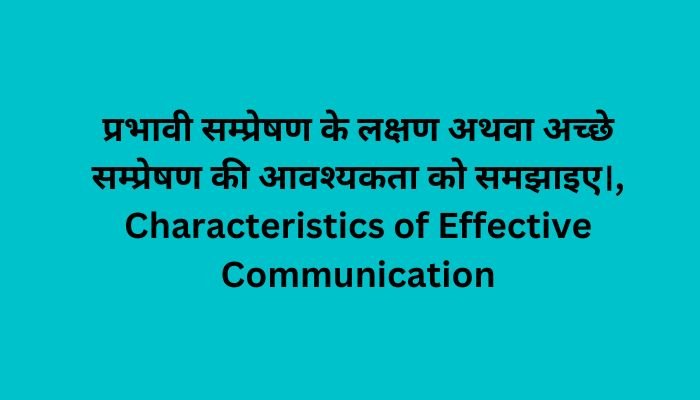
प्रभावी सम्प्रेषण के लक्षण
संदेशवाहन की सार्थकता केवल समाचारों के सम्प्रेषण में निहित नहीं है, अपितु संदेश के प्राप्तकर्त्ता पर इससे हुए प्रभाव पर निर्भर करता है। जब कोई संदेश किसी व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है तो इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। यदि संदेश इस प्रकार से सम्प्रेषित किया गया है कि जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाये तो हम इसे प्रभावी संदेशवाहन कहेंगे।
संक्षेप में एक अच्छे सम्प्रेषण की आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं-
(1) स्पष्ट संक्षिप्त एवं परिपूर्ण कथन – संदेशवाहन की स्पष्टता के लिए सूचनाकर्त्ता को स्वयं तत्सबंधी सभी बातों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। स्पष्ट संदेश को समझने में संदेश प्राप्तकर्त्ता को व्यर्थ समय नहीं खोना पड़ता है। संदेशवाहन की संक्षिप्तता से तात्पर्य शालीनहीनता। या अभद्रता कदापि नहीं है। इसके अतिरिक्त संदेश संक्षिप्त होने के साथ-साथ कथ्य-तथ्य की दृष्टि से परिपूर्ण होना चाहिए। एक ही संदेश या संवाद के लिए बार-बार पूछताछ तथा उत्तर प्रत्युत्तर की आवश्यकता न हो।
(2) समुचित सम्प्रेषण विधि-संदेश की भाषा कितनी ही मधुर एवं शालीन हो, यदि सम्प्रेषण विधि अभद्र हो तो इससे भी संदेश प्राप्तकर्त्ता के आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचने का भय है। तब संदेशवाहन का प्रयोजन ही असफल हो जायेगा। संवाद सम्प्रेषण की कोई एक निर्धारित विधि नहीं है वस्तुत: यह संदेश भेजने वाले एवं प्रापक के पद स्तर, अवसर एवं प्रचलित रीतियों पर निर्भर करेगा।
(3) संदेशवाहन भविष्य दृष्टा हो— यद्यपि संदेशवाहन वर्तमान आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। किन्तु दूरदर्शी प्रबंधक संदेशवाहन में भावी सम्भावनाओं की भी उपेक्षा नहीं करते। वस्तुतः प्रभावी संदेश वाहन पद्धति तो वह होगी जो न केवल विद्यमान समस्याओं के समाधान में ही सहायक हो अपितु जो भावी सम्भावनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सके।
(4) शिष्टता एवं शालीनता-सम्प्रेषण को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यह शिष्ट, मधुर एवं शालीन हो। विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, किन्तु इसक तात्पर्य यह नहीं है कि इससे अभीष्ट प्रभाव ही उत्पन्न न हो। कथन की यथार्थता बनाये रखने के लिए यदि भाषा में कुछ कठोरता लानी पड़े तो यह परिस्थिति अनुकूल होगा।
(5) पारस्परिक सहयोग—अच्छे सम्प्रेषण के लिए संदेश देने वाले एवं संदेश प्राप्तकर्त्ता के मध्य मिल जुलकर संदेशानुकूल कार्य करने की भावना की आवश्यकता है। यदि संदेश ग्रहण हो न किया जाये तो वह व्यर्थ हो जावेगा। संदेश का सम्प्रेषण जितना महत्त्वपूर्ण है, उतनी ही महत्त्वपूर्ण इसकी प्राप्ति भी है। संदेश प्रभावकारी हो एवं इसके अनुसार क्रियान्वयन हो, इसके लिए संदेश की भाषा और इसमें सन्निहित भावना शिष्ट, शालीन एवं सम्मानपूर्वक होनी चाहिए. तभी संदेश को प्राप्तकर्त्ता से संदेश के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जा सकती है।
(6) निर्बाध एवं निरन्तर होना- व्यावसायिक सम्प्रेषण का अब महत्त्व पूरी तरह अंगीकार किया जाने लगा है। इसका क्षेत्र भी एक पक्षीय से द्विपक्षीय तथा द्विपक्षीय से तृतीय पक्षीय हो गया है। सम्प्रेषण संबंधित पक्षकारों के बीच निर्वाध गति से सतत् चालू रहना चाहिए जिससे निरन्तर विचारों के आदान-प्रदान का लाभ प्राप्त हो सके।
(7) संदेश के सम्प्रेषण के पूर्व पर्याप्त विचार-अच्छे एवं प्रभावी सम्प्रेषण के लिए आवश्यक लक्षण है कि सम्प्रेषण किये जाने वाले संदेश पर पर्याप्त पूर्व विचार कर लिया जाये घबराहट में अधूरी अवस्था में अथवा अविवेकपूर्ण सम्प्रेषण सदैव आपत्तिजनक होता है और इस पर किया जाने वाला व्यय निरर्थक भी हो जाता है। अतः जार्ज आर. टैरी ने कहा “संदेश भेजने से पूर्व जो कुछ वह भेज रहा है, उस पर प्रेषक को स्पष्ट विचार तथा स्थिति का ज्ञान होना चाहिए।”
(8) आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना सम्प्रेषण उचित आदर्श प्रस्तुत कर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस संबंध में अंग्रेजी की कहावत Example is better than precept सही-सही लागू होती है। यदि हम यह चाहते हैं कि कर्मचारी किन्हीं निर्देशित नियमों का उचित रूप से पालन करें तो उन नियमों का स्वयं पालन कर हमें आदर्श दृष्टान्त प्रस्तुत करना चाहिए। प्रायः समय पर कार्यालय में उपस्थित होने के आदेश सभी कार्यलय में बार-बार प्रसारित किये जाते हैं। किन्तु अधिकारी स्वयं समय पर कार्यालय में नहीं पहुँचते। ऐसी दशा में इस आदेश का पूरा-पूरा पालन होगा, इसमें संदेह ही है।
(9) मधुर संबंध एक अच्छी सम्प्रेषण प्रणाली को अपनाकर व्यवसाय के स्थायी प्रबंधक, कार्यकर्त्ता एवं जनता के मध्य विचारों के निरन्तर आदान-प्रदान द्वारा आपसी समस्याओं का समाधान हो जाता है जिससे संबंधों के मधुर बनाने में सहायता प्राप्त होती है। किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि इन सभी पक्षकारों के बीच मधुर एवं सम्मानपूर्व संबंध होने पर संदेशानुकूल आचरण भी अधिक संभव है वस्तुतः मधुर संबंधों के कारण कुछ असुविधा होते हुए भी संदेशानुसार आचरण संदेश प्रापक करता ही है।
(10) अनुवर्तन सम्प्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए उसका निरन्तर अनुवर्तन (Follow- up) होते रहना, आवश्यक है। अनुवर्तन की गति क्या हो ? यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। की प्रभाविता के विषय में संदेश के परिणामों का सामयिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। संदेश को निष्फल बनाने वाले कारणों का सही सही पता लगाकर उनका निराकरण किया जाये। किन्तु अनावश्यक अनुवर्तन द्वारा प्रेषित को क्रुद्ध करने का भी भय होता है। अत: अनुवर्तन सामयिक एवं उपयुक्त प्रवृत्ति का होना चाहिए।
