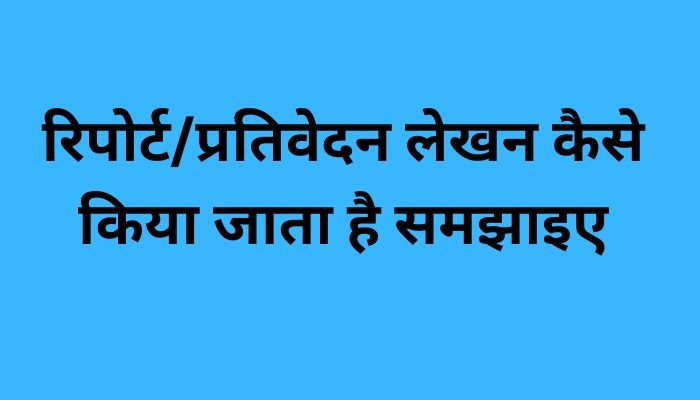
रिपोर्ट/प्रतिवेदन लेखन कैसे किया जाता है समझाइए
यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि रिपोर्ट/प्रतिवेदन लेखन कैसे किया जाये ? इसके प्रत्युत्तर में यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि किसी भी निर्णय के संबंध में प्रतिवेदन लिखते समय चतुरता एवं कुशाग्रता महत्त्वपूर्ण है। इसलिए इसे पूर्व बातों को ध्यान में रखकर एवं भली-भांति सोच-समझकर लिखा जाना चाहिए। ऐसा न करने पर एक और विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे तो दूसरी ओर लेखक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, साथ ही अनेक निराशाएँ देखने को मिलेंगी अतः प्रतिवेदन इस प्रकार लिखा जाना चाहिए-
(1) प्रतिवेदन लिखने का उद्देश्य सर्वप्रथम लेखक को यह पता करना चाहिए कि प्रतिवेदन क्यों लिखा जा रहा है ? यदि व्यावसायिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसके उद्देश्य एवं व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि प्रतिवेदन लिखने का उद्देश्य प्रबंधक को विभिन्न बातों की जानकारी देना है तो इससे संबंधित सभी जानकारियाँ स्वयं के पास होनी आवश्यक हैं। ऐसा होने पर भी प्रतिवेदन लिखने में काफी सुविधा हो जाती है।
(2) आँकड़ों की प्राप्ति एवं उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण करना – प्रतिवेदन लेखन एवं उसके उद्देश्य की जानकारी हेतु आँकड़ों को प्राप्त किया जाता है। ये आँकड़े अभिलेखों एवं पुरानी फाइलों से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके पश्चात् उन आँकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए। इस संबंध में विश्लेषकों को बड़े धैर्य एवं निपुणता से कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से आँकड़ों का सही विश्लेषण हो सकेगा और अगले व्यक्ति को सम्प्रेषित करने में आसानी रहेगी।
(3) रूपरेखा तैयार करना—उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् रिपोर्ट लेखक कुछ नोट्स तैयार करता है ताकि रिपोर्ट लिखने में सुविधा हो। अतः रिपोर्ट लिखने के पूर्व यह विचार करना आवश्यक है कि उसे कहाँ-कहाँ से लिखना आरम्भ किया जाये, उसकी विषय-सामग्री क्या होगी और उसे अंतिम रूप किस प्रकार दिया जायेगा। इसके लिए तथ्यों का संक्षिप्त रूप में विश्लेषण किया जाना आवश्यक है तभी उचित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकेगा।
(4) प्रतिवेदन को व्यवस्थित क्रम प्रदान करना- समस्या को परिभाषित करने के पश्चात् प्रतिवेदन को उचित, व्यावहारिक एवं समय को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित क्रम प्रदान करने का कदम आता है। इसके लिए निम्नलिखित सहायताएँ प्राप्त की जाती हैं-
(i) उपयोगी, सार्थक एवं आधारभूत सिद्धान्तों का उपयोग किया जाना चाहिए।
(ii) समस्या को विभिन्न चरणों में विभाजित करके प्रस्तुत करना चाहिए।
(iii) यहाँ यह कोशिश की जानी चाहिए कि समस्या का प्रत्येक पक्ष एक-दूसरे से पृथक् एवं स्पष्ट हो ।
(iv) प्रतिवेदन के वर्गीकरण की उचित तकनीक का प्रयोग करना चाहिए।
(v) प्रतिवेदन में विभिन्न तर्क प्रस्तुत करने चाहिए।
(vi) प्रत्येक समस्या से संबंधित आँकड़े भी प्रस्तुत करने चाहिए।
(5) संगृहीत सूचनाओं का गहन अध्ययन करना— प्रतिवेदन लेखन के इस चरण में उपर्युक्त समस्याओं से संबंधित संगृहीत सूचनाओं का गहन अध्ययन किया जाता है। इसके लिए प्रतिवेदन लेखक शोधों की जाँच करता है। इसके लिए विभिन्न माध्यमों से जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए। परिणामस्वरूप वांछित निष्कर्षो की प्राप्ति की जा सके और अच्छे सुझावों, सिफारिशों की उत्पत्ति की जा सके। इस प्रकार अच्छी सिफारिशें सदैव पाठक के लिए स्वीकार्य योग्य एवं अत्यधिक व्यावहारिक होगी।
(6) रिपोर्ट लिखना एवं प्रेषित करना- अंत में, रिपोर्ट लेखक शीर्षक बनाकर उसे लिखता है। तत्पश्चात् अपने हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार रिपोर्ट लिखी जाती है।
